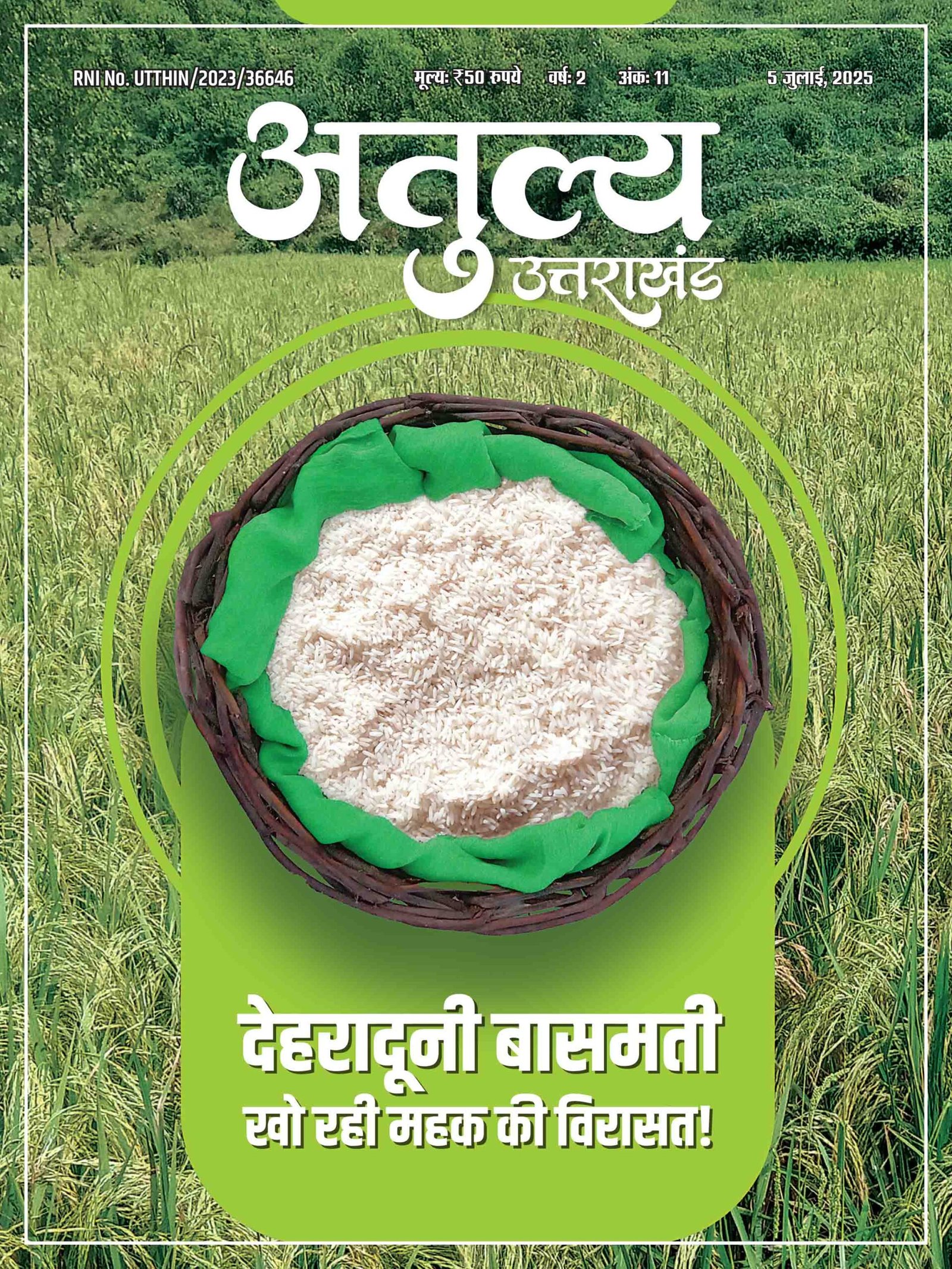इसमें दो राय नहीं है कि स्थानीय बोलियां संकट में है। जैसे-जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्र घट रहा है, उसी के साथ देश के हर हिस्से में क्षेत्रीय बोलियों का चलन कम होता जा रहा है। हर जगह बोली की पहचान ओर दायरा सिकुड़ रहा है। उत्तराखंड का संकट बाकी हिस्सों से बड़ा है, क्योंकि यहां पलायन बड़ा संकट है। यानी, गांव खाली होते जा रहे हैं। ऐसे में क्षेत्रीय बोलियां विलुप्त होने लगी हैं। अगर बोलियां जाएंगी तो अपने साथ कई चीजों को ले जाएंगी। इसका असर लोक परंपराओं पर भी पड़ेगा। असर दिखने भी लगा है। इसी मुद्दे पर अतुल्य उत्तराखंड के संपादक अर्जुन सिंह रावत की जाने माने कवि एवं लेखक महेश पुनेठा से विशेष बातचीत के प्रमुख अंश…
दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, ऐसे में हम ग्लोबल लैंग्वेज की बात करते हैं, उसमें अपनी दूधबोली को संभाले रखना, अपनी विरासत को बचाए रखना, कैसे होगा?
यह संकट पूरी दुनिया में पैदा हुआ है। कहा जाता है कि हर रोज कोई न कोई बोली मर रही है। बहुत सारी बोलियां पूरी तरह से खत्म हो चुकीं हैं। इसका कारण है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। एक तरह से यह लोक का दुश्मन भी है। पूरी दुनिया को एक तरह की बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में लोकबोली, लोकसंस्कृति और लोकजीवन को बचाना अपने आप में एक चुनौती है। यह सब जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं और जीवन तेजी से बदल रहा है। जहां से बोली का संबंध है, वह सब बदल रहा है। आज हमारे गांव खाली हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है उनके साथ गांव की संस्कृति, बोली पर भी खतरा बढ़ गया है।
बोली बचाने का सवाल एकाकी नहीं…
बोली बचाने का सवाल एकाकी नहीं है। बोली तमाम क्रियाओं से जुड़ी होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब जीवन बचेगा तो बोली बचेगी। आप देखिए, कोरोना काल आया। कितने नए शब्द पैदा हुए। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जो हमारे लोक जीवन के क्रियाकलापों से पैदा हुए। व्यंजनों से पैदा हुए, अनाजों से पैदा हुए, खेती के कामकाजों से पैदा हुए, औजारों से पैदा हुए। जब वो काम ही नहीं रहे, तो उनसे जुड़े हुए शब्द कैसे रहेंगे। ऐसे में उस बोली को बचाना बड़ा कठिन काम है। मुझे लगता है कि एक बड़ी संगठित लड़ाई की जरूरत है।

बाजार, रोजगार की भाषा ही बढ़ेगी…
कोई बोली या भाषा तब अधिक विस्तार पाती है, जब वह बाजार की भाषा बन जाती है। जब वह रोजगार की भाषा होती है। आज अंग्रेजी का जो वर्चस्व है उसका कारण यह नहीं है कि लोगों को उससे बड़ा लगाव है। अंग्रेजी का प्रभाव इसलिए बड़ा है क्योंकि यह रोजगार की भाषा है। कोई अच्छा काम पाना है तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। आपको किसी दूसरे देश में जाना है या व्यापार करना है तो आपको अंग्रेजी आनी ही चाहिए। इसलिए लोग अंग्रेजी सीखने के लिए जी जान लगा देते हैं। पूरी दुनिया में इसलिए अंग्रेजी का खूब विस्तार हुआ।
मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं के सामने भी खतरा?
हिंदी माध्यम या अन्य भारतीय भाषाई माध्यमों के स्कूल खाली होते जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं के सामने भी खतरा उत्पन्न हो गया है। हिंदी के सामने खतरा आने लग गया है। आप देखेंगे कि अगले 10 साल बाद हम इसी तरह हिंदी बचाने के बारे में बात कर रहे होंगे, जिस तरह से आज हम लोक बोलियों के बारे में बात कर रहे हैं। माध्यम भाषा के रूप में अब हिंदी धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। अपनी भाषाओं को हम कैसे बचाएं। मुझे लगता है इसके लिए हमें सामूहिक स्तर पर प्रयास करने होंगे। व्यवहार में जितना इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। अपनी बोली में अच्छा साहित्य सृजित किया जाए। यदि हमारी बोली में अच्छा साहित्य लिखा जाए तो उसको पढ़ने के लिए लोग प्रेरित होंगे। जब उसे लोग पढ़ेंगे तो बोली बची रहेगी। अपनी दूधबोली को बचाने की लड़ाई इस तरह भी लड़ सकते हैं।

जौनसारी, रं बोली बचाने की बात भी करनी चाहिए….
मैं कहता हूं, भाई केवल आप हिंदी को बचाने की बात क्यों करते हैं। कुमाऊंनी या गढ़वाली को ही बचाने की बात क्यों करते हैं? आपको जनसारी को बचाने की बात भी करनी पड़ेगी। आपको रं भाषा को भी बचाने पर बात करनी पड़ेगी। सबको मिलकर यह लड़ाई लड़नी होगी। सारी भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी के वर्चस्व के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। भावनात्मक रूप से हमें अपनी बोली के प्रति प्रेम है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन, इतने भर से बात नहीं बनेगी। धीरे-धीरे वह कम होती जाएगी। जब तक राजनीतिक स्तर पर इसे बचाने के लिए कोई ठोस फैसले नहीं होते हैं, तब तक इसे बचाना कठिन काम होगा।
भाषा का सरलीकरण सही है या गलत ?
भाषा का सरलीकरण बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि यदि आज अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा बनी है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि अंग्रेजी भाषा की उदारता है। उसने हर भाषा के शब्दों को अपने शब्दकोश में शामिल किया है। यदि हम शुद्धता की बात करेंगे, शुद्धतावाद पर चलेंगे, हम कहेंगे- नहीं-नहीं हम दूसरी भाषाओं के शब्द हमारे बोली-भाषा में नहीं लिए जाएंगे तो ऐसा करके हम कहीं ना कहीं अपनी भाषा के प्रसार को ही रोकेंगे। हमें दूसरी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करना ही चाहिए। और उसको सहज-सरल बनाने की भी जरूरत है। उसमें बहुत रुढ़िवादी होने की जरूरत नहीं है। यह बहुत जरूरी है भाषा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए। अपनी भाषाओं के दरवाजे हमें खोलने पड़ेंगे। उसकी खिड़कियां हमें खुली रखनी पड़ेंगी। ताकि, बाहर की हवा भी वहां आए और हमारे यहां से ही बाहर जाए। ये बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा, मैं लिखता जरूर हिंदी में हूं। लेकिन, मेरी कविताओं में स्थानीय बोली के शब्द जरूर होते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बहाने हिंदी में हमारी बोली के शब्द समाविष्ट हो, जैसे भोजपुरी, अवधी आदि के शब्द आप हिंदी में देखते हैं। खड़ी बोली में बहुत सारी भाषाओं के शब्द होते हैं। हमारी बोली के शब्द भी वहां पहुंचने चाहिए। इस तरह से हम अपनी दूधबोली भाषा की सेवा कर सकते हैं। उसे आगे बढ़ा सकते हैं। जो एकडमिक लोग हैं वे लुप्तप्राय शब्दों को शब्दकोश में संरक्षित कर दूधबोली को बचाने में सहयोग कर सकते हैं।
बोली पर होने वाली चर्चा बहुत ज्यादा एकेडमिक होती है, इसकी वजह से यूथ कनेक्ट फील नहीं कर पाता, क्या कहेंगे?
जी बिलकुल, इसके लिए ही बोली-भाषा बचाने वाले आंदोलनों-अभियानों बड़ी अहमियत है। इससे हम भावनात्मक रूप से उसे आकर्षित करते हैं। उनको झकझोरते हैं। गढ़वाली, कुमाऊंनी भाषा बचाने का अभियान चलता है, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं। सिर्फ, कुमाऊंनी या गढ़वाली बचाने की ही बात क्यों करते हो। उत्तराखंड में 13 बोलियां हैं। उनका भी तो अपना महत्व है। हमें इन सभी को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। सामूहिक प्रयास से ही सब बचेंगे।